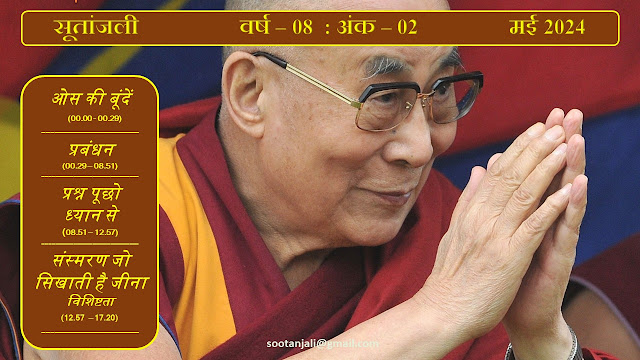धन्यवाद
इस
माह हम छह वर्ष पूर्ण कर सातवें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं।
यह
आपके स्नेह और सुझावों के कारण ही संभव हो
सका है।
आप
से एक ही अनुरोध है, मेल, ब्लॉग या
व्हाट्सएप्प पर संपर्क बनाए रखें और
अपने
सुझावों से हमारा मार्गदर्शन करते रहें।
*****
गलतियों
को मुद्दा बना कर टकराव को बढ़ाने के बजाय
गलतियों
का अहसास करवाकर
स्वस्थ्य
मिसाल कायम करना ही शुभ होता है।
------------------ 000
----------------------
सुख की खोज में कोलंबस चिंतन
पूरी दुनिया का
चक्कर लगाने के बाद कोलंबस इसी नतीजे पर पहुंचा,
“सुख पाने के लिए हमें कुछ और नहीं बस सही स्याही चाहिए”। नहीं समझे! जिस सुख को
खोजने हम दर-दर भटकते हैं, उसे खोजने बड़ी यात्रा पर जाने की जरूरत
नहीं है, वह हमारे इर्द-गिर्द ही है। आइए, समझने का प्रयत्न करते हैं, अलग-अलग माध्यम
से।
कम्युनिस्ट दौर का
एक पुराना किस्सा है। पूर्वी जर्मनी से एक आदमी को साइबेरिया भेजा गया। उसको मालूम
था कि उसके पत्र-व्यवहार पर विरोधियों की नजरें रहेगी। इसलिए उसने अपने मित्रों से
कहा कि क्यों न एक कोड बना लिया जाये। मैं अपनी चिट्ठी अगर नीली स्याही से लिखूं,
तो समझना कि जो कुछ भी मैंने लिखा है, वह सब
सच है और अगर काली स्याही से लिखूं, तो समझना कि मेरी लिखी
हर बात झूठ है। कुछ समय बाद उसने अपने दोस्त को नीली स्याही से चिट्ठी लिखी,
'यहां हर चीज़ भव्य है। दुकानें, खाने-पीने की
उम्दा चीजों से भरी हुईं हैं। सिनेमाहॉलों में बढ़िया फ़िल्में दिखाई जाती हैं।
मकान बड़े-बड़े और शानदार हैं और उनमें रहने वाले लोग सहृदय हैं। यहां मुझे कोई असुविधा
नहीं है, सिवाय इसके कि लाख चाहूं, तो
भी लिखने के लिए काली स्याही नहीं ख़रीद सकता...'।
हमारा समय ऐसा ही
है। हमारे पास सत्य, न्याय, नीति, नैतिकता और आदर्शवाद का ढेर है, पर उन्हें लिखने के
लिए सही स्याही नहीं है, पढ़ने के लिए सही भाषा नहीं, समझने के लिए सही मस्तिष्क नहीं। अध्यात्म हमें इस सही स्याही को जुटाने और जीवन की चिट्ठी
को एक बार फिर से लिखने का अवसर देता है। देखना यह कि हममें से कितने इस ख़त को
लिखने के लिए सही स्याही चुनते हैं, पढ़ने के लिए सही भाषा
इस्तेमाल करते हैं और समझने के लिए सही मस्तिष्क रखते हैं।
चेखव की एक कहानी
है – “वार्ड नंबर सिक्स”। इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं- रेगिन और ग्रोमोव।
मेडीकल रिपोट्र्स के मुताबिक़ ग्रोमोव विक्षिप्त है, लेकिन उसकी बातें उसे बुद्धिमान साबित करती हैं। वह अन्याय, झूठ, पिछड़ेपन और आडंबर से घिरे जीवन को लेकर दुख और
आक्रोश से भरा है। वह डॉ. रेगिन से कहता है कि देखो, हर ओर
कैसी घुटन है। जो सक्षम हैं, वे निष्क्रिय और दुराग्रही हैं।
जो कमज़ोर हैं, वे अज्ञान और पाश्विकता से भरे हैं। हम महज
कंगाल हैं, क्योंकि भीड़ग्रस्त हैं। पतनशील हैं। नशे में,
दिखावे में और झूठ में आवृत्त हैं। फिर भी घरों और सड़कों पर
ख़ामोशी है। हजारों लोग हैं, पर इस सब के लिए कोई नहीं चीखता।
लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो
रहे हैं, मूर्खतापूर्ण बातें बना रहे हैं, ब्याह शादी रचा रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। ख़ुद को
लगातार क़ब्रों की ओर ढो रहे हैं, पर जीवन की तकलीफ़ों को
नहीं सुन पा रहे...। तब रेगिन उससे कहता है कि अगर सुखी रहना चाहते हो, तो हर बुराई को नजरंदाज (इग्नोर) करो। अन्याय को भी और झूठ को भी, पाप को भी। लेकिन उसका यही दर्शन एक रोज ख़ुद उसे वार्ड नंबर सिक्स का
मरीज बना देता है। क्या आपको नहीं लगता कि जिसे महत्व देना चाहिए उसे ही नजरंदाज
कर रहे हैं?
न्यूरोसाइंस के मुताबिक़
जीवन की वे सभी बातें जिन्हें हमने अपनी उथली प्रगति और आधुनिकता बोध के कारण
अकल्पनीय-सा बना लिया है, अब वक़्त आ गया है कि उन्हें जीवन
को लौटाया जाए। अंधेरों की खाई में गिरते जीवन की रक्षा के लिए अब यही एक उपाय है
कि हम अपने मनुष्यत्व के खोए हुए अर्थ तलाशें। अपनी सहजता की ओर लौटें। उन
छोटी-छोटी चीजों से जुड़ें, जिन्हें बड़ा बनने की आपाधापी
में हम झटककर चले आए हैं। न्यूरोसाइंस दरअसल हमें उस चरवाहे की याद दिलाना चाहता
है, जो हमारे पुरखों की कहानियों में अब तलक मजे से बांसुरी
फूंक रहा है।
एक रोज उस चरवाहे से किसी ने पूछा कि बताओ आज मौसम कैसा रहेगा?
सवाल सुनकर चरवाहा मुस्कुरा दिया, मानो यही
जवाब हो। पूछने वाले ने दोबारा पूछा, 'हंसो मत ये बताओ आज
मौसम कैसा रहेगा?" चरवाहा बंसी में सुर फूंकते-फूंकते
रुका और बोला, 'जैसा मैं चाहूंगा,
वैसा।'
'मतलब?'
'मतलब ये
कि मौसम तो हर हाल में वैसा रहेगा जैसा धरती चाहेगी, पर मेरे
मन का मौसम वैसा रहेगा, जैसा मैं तय करूंगा।'
उस दिन पूछने वाले को एक नया सबक मिला कि अगर तुम भीतर का
मौसम बदल सको तो बाहर का मौसम अपने आप बदल जाता है।
गोर्की ने
न्यूयॉर्क को देखकर जिस सोना निगलने वाले एक पीले दैत्य की कल्पना की थी,
वह दैत्य भारत के मन में भी आकार ले रहा है। हम एक ऐसा समाज बन रहे
हैं, जिसके मन में पूंजी की भूख निरंतर गहरा रही है। लोग
धरती, आकाश, समुद्र, हवा, वनस्पति, सब-कुछ को मसलकर
पूंजी के ढेर में बदल रहे हैं और जीवन को एक नितांत रूखी, ठंडी,
संवेदनहीन चीज में। और सबसे दुखद बात यह है कि हम, प्रगतिशील दुनिया के लोग, यह भी नहीं जानते कि हम चाहते
क्या हैं, पर अपनी अनिश्चित मांग को पूरा करने के लिए हमने
अपने जीवन को नरक बना रहे हैं।
इन दिनों जीवन
इसलिए जटिल है, क्योंकि अपनी प्रगतिशीलता को हांकने की जल्दबाजी
में हमने सच्चाई और सरलता को हाशिए पर रख दिया है। आधुनिक होने की आतुरता में हमने
पुरातनता को तो बड़ी तेजी से विस्मृत किया, पर कुछ नया नहीं
रच पाए। हमने शिल्प और कलाओं से लेकर प्रकृति और पर्यावरण तक हर चीज का विनाशकारी
दोहन किया, पर उनकी नई पौध रोपने की मोहलत नहीं तलाशी। नए
समय ने सब के हाथों में मोबाइल तो दे दिया, पर ऐसा कोई आदर्श,
कोई मूल्य वह नहीं दे पाया, जिसे सवा अरब
आबादी का मन अपना पाता।
स्टीवेन लेविट
अपनी पुस्तक 'फ्रेकोनोमिक्स' में लिखते हैं
कि नैतिकता या आदर्श वे चीजें हैं, जिनसे हम समाज को सजा हुआ
देखना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक जगत उस संसार का चित्र दिखाता
है, जैसा हमने इसे बना लिया है। एक ऐसे समाज में जहां हर चीज
बिकाऊ है, यह एक बड़ा मुद्दा है कि ज्यादा धन से
ज्यादा खुशियां मिलती हैं या खुशियों का अभाव होता है? सरलता आती है या जटिलता आती है?
अपनी अर्थव्यवस्था
को अगर उदात्त अर्थों से भरना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक नया पूंजीवाद चाहिए,
जो स्वार्थी नहीं सहृदय हो। आज दुनिया भर के अर्थशास्त्री पूंजी के
नए मायने तय कर रहे हैं। उनकी इस नई परिभाषा में सबसे ऊपर है- मानवीय पूंजी
यानी मनुष्य। दूसरे नंबर पर है- सामाजिक पूंजी यानी रिश्ते, तीसरे पर है- प्राकृतिक पूंजी यानी पर्यावरण, चौथे पर- मानवनिर्मित पूंजी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे निचले
पायदान पर आर्थिक पूंजी यानी मुद्रा । 2010 में हुए
एक शोध में यह निष्कर्ष दिया गया कि किसी भी समाज के सुख का मुख्य कारण वैयक्तिक
पूंजी नहीं, सामाजिक जुड़ाव है। पर विडंबना यह है कि हमारी
दौड़ इस आख़िरी पायदान, पूंजी पर आकर ठहर गई है।
महात्मा गांधी ने
जब कहा कि यंत्र और उद्योग की परवशता और उससे जन्मी अर्थ पिपासा का इलाज होना
चाहिए, तब वे भी हमें विकास, प्रगति
और सुख के उन्हीं मायनों पर पुनर्विचार के लिए ही आगाह कर रहे थे जिनके लिए आज
विज्ञान कह रहा है। शायद वे समय से काफी आगे चल रहे थे। आदर्श और व्यवहार को दो
अलग-अलग चीजें मानकर हम जीवन का खेल यह सोचकर खेले जा रहे हैं कि हम बड़े
बुद्धिमान हैं, लेकिन ऐसा करते हुए हम महज ‘वार्ड नंबर सिक्स’ का विस्तार ही कर रहे हैं।
अगर हम आदर्श और
अर्थ के बीच की खाई (गैप) को भरना चाहते हैं, तो
उसके लिए जरूरी है कि हम देना शुरू करें। पूरे दिन को छोटी-छोटी देनों से भर दें। जरूरत
पड़ने पर खुद का नुकसान कर के भी दें। पर याद रखें कि दान का सरोकार सिर्फ़ धन से
नहीं है। ज्ञान, अनुभव, प्रज्ञा,
भावना, कलाएं, पर्व,
भाषाएं यहां तक कि समय, स्पर्श, विश्वास और क्षमा भी... जीवन में सब-कुछ लेना-देना ही तो है। पेड़ लगाना
भी देना ही है। किसी को सड़क पार करा देना भी। किसी की तक़लीफ़ को सुन लेना भी
देना है और मुस्कराना भी...
मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा द्वितीय विश्वयुद्ध की एक घटना से। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, लिथुआनिया में एक जापानी राजनयिक चिउनेसुगिहारा तैनात थे। एक सुबह उनकी नींद दूतावास के बाहर जमा हुए हजारों लोगों के शोर से खुली। उन्हें बताया गया कि वे यहूदी थे जो हिटलर के हाथों मौत से बचने
के लिए पोलैंड से भाग गए थे और जापान जाने के लिए वीज़ा चाहते थे। एक बार में हजारों वीजा देना और वह भी शरणार्थियों को, एक गंभीर मुद्दा था और इसलिए उन्होंने अपनी सरकार से सलाह ली। वे टेलेक्स संदेशों के दिन थे। पहला संदेश, उत्तर था 'नहीं'; दूसरा संदेश, उत्तर 'नहीं' था; तीसरे संदेश में, जैसा कि अपेक्षित था, उत्तर अभी भी 'नहीं' था। उनका आधिकारिक कर्तव्य अपनी सरकार के निर्देशों का पालन करना था। लेकिन उनकी आंतरिक आवाज ने उनसे कहा कि वह अपने पद का उपयोग इन लोगों को मौत से बचने में मदद करने के लिए करें। उन्हें वीज़ा जारी किया गया, जापान वापस बुलाया गया, लेकिन वे हज़ारों लोगों की जान बचाने में सफल रहे। उन्हें जापान में अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें जो मिला वह माप से परे था - देने की खुशी, स्थायी मानसिक शांति और संतुष्टि।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
हिसाब, पर्यावरण का लघु कहानी - जो सिखाती
है जीना
कस्तूरी
सारे शहर में जहां-तहां घूमता रहता था, जैसे
कुछ ढूंढ रहा हो। फिर आ गया और बोला, “दुनिया पर मेरा कुछ
निकलता है, कोई हिसाब कर दें’।
कस्तूरी पागल था, इसलिए कोई उसका हिसाब नहीं करता था। बस खाने-पीने को कुछ दे दिया जाये, तो वह चला जाता। एक दिन मैंने मज़ाक में कहा, ‘कस्तूरी आज मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा, बोलो क्या
बाकी है दुनिया पर?’ निकालो रुक्का,
लालकिला चाहिये, की ताजमहल?’
वह खुश हो गया और बोला, ‘मेरे पास एक नदी थी, वह कहाँ
गई? एक जंगल था। कौन ले गया? मेरे
पाखी-परेबा कहाँ गये?’
मैं अकबकया, ‘यह कोई कैसे बताएगा?’
‘फिर मेरा हिसाब रहने दो’, वह दुखी होकर बोला।
कुछ पल कि चुप्पी के बाद मैंने कहा,
‘अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है, कस्तूरी?’
‘मालूम नहीं भूल गया हूँ।’
‘घर में और लोग थे?’
‘थे, बहुत लोग थे बाबू।’
‘वे लोग अब कहाँ हैं?’
‘क्या पता! उसने हाथ हिलाया।’
‘पागल कैसे हो गये?’, मैं असली सवाल पर आया।
‘दुनिया की चाल से’, उसने कुछ सोचकर कहा।
‘ठीक कैसे होगे?’
‘हिसाब मिलने पर।’
कस्तूरी
एक समय के बाद काफी बूढ़ा हो कर मर गया। वह पागल क्यों हुआ? ठीक-ठीक कोई अनुमान नहीं कर सका। वैसे मुहल्ले के
बड़े-बुजुर्ग आज भी यही कहते हैं कस्तूरी की तरह आदमी सोचने लगे तो
...................
(संजय सिंह)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
आपको सूतांजली पसंद आ रही है, आप चाहते हैं दूसरों को भी पढ़ना चाहिए।
तो इसे लाइक करें, सबस्क्राइब करें, परिचितों से शेयर करें।
अपने सुझाव ऑन लाइन दें।
यू
ट्यूब पर सुनें : à